ज्योतिबा फुले
जन्म: 11 अप्रैल, 1827
जन्म स्थान: सतारा, महाराष्ट्र
माता-पिता: गोविंदराव फुले (पिता) और चिमनाबाई (मां)
पत्नी: सावित्री फुले
बच्चे: यशवंतराव फुले (दत्तक पुत्र)
शिक्षा: स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल, पुणे;
संघ: सत्यशोधक समाज
विचारधारा: उदारवादी; समतावादी; समाजवाद
धार्मिक विश्वास: हिंदू धर्म
प्रकाशन: तृतीया रत्न (1855); पोवाड़ा: छत्रपति शिवाजीराजे भोंसले यंचा (1869); शेटकरायच आसुद (1881)
निधन: 28 नवंबर, 1890
स्मारक: फुले वाडा, पुणे, महाराष्ट्र

ज्योतिराव या ज्योतिबा ’गोविंदराव फुले भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक और उन्नीसवीं सदी के विचारक थे। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति-प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह किया और किसानों और अन्य निम्न-जाति के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत में महिला शिक्षा के लिए भी अग्रणी थे और उन्होंने जीवन भर लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। माना जाता है कि वह दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए अनाथालय शुरू करने वाला पहला हिंदू था।
बचपन और प्रारंभिक जीवन:-
ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनके पिता, गोविंदराव पूना में एक सब्जी विक्रेता थे। ज्योतिराव का परिवार 'माली' जाति का था और उनका मूल शीर्षक 'गोरही' था। मालियों को ब्राह्मणों द्वारा एक नीच जाति के रूप में माना जाता था और सामाजिक रूप से दूर किया जाता था। ज्योतिराव के पिता और चाचा फूलवाले के रूप में सेवा करते थे, इसलिए परिवार को `फुले 'के नाम से जाना जाने लगा। ज्योतिराव की माँ का निधन हो गया जब वह सिर्फ नौ महीने के थे।
ज्योतिराव एक बुद्धिमान लड़का था लेकिन घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसे कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। उसने परिवार के खेत में काम करके अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया। बच्चे के कौतुक की प्रतिभा को पहचानते हुए, एक पड़ोसी ने उसके पिता को उसे स्कूल भेजने के लिए मना लिया। 1841 में, ज्योतिराव ने स्कॉटिश मिशन के हाई स्कूल, पूना में दाखिला लिया और 1847 में अपनी शिक्षा पूरी की। वहाँ उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण सदाशिव बल्लाल गोवन्दे से हुई, जो जीवन भर उनके करीबी दोस्त रहे। मात्र तेरह वर्ष की आयु में, ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था।
सामाजिक आंदोलन:-
1848 में, एक घटना ने ज्योतिबा के जातिगत भेदभाव के सामाजिक अन्याय के खिलाफ खोज की और भारतीय समाज में एक सामाजिक क्रांति को उकसाया। ज्योतिराव को अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था जो एक उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार से था। लेकिन शादी में दूल्हे के रिश्तेदारों ने ज्योतिबा का अपमान किया और उनका अपमान किया जब उन्हें उसकी उत्पत्ति के बारे में पता चला। ज्योतिराव ने समारोह छोड़ दिया और प्रचलित जाति-व्यवस्था और सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देने का मन बना लिया। उन्होंने सामाजिक प्रमुखता के वर्चस्व के लक्ष्य को पूरी तरह से दूर करने के लिए अपने जीवन का काम बना लिया और इसका उद्देश्य उन सभी मनुष्यों को मुक्त करना था जो इस सामाजिक अभाव के अधीन थे।
थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक 'द राइट्स ऑफ मैन' को पढ़ने के बाद, ज्योतिराव उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने के लिए महिलाओं और निम्न जाति के लोगों का ज्ञान ही एकमात्र उपाय था।
सामाजिक आंदोलन:-
महिला शिक्षा की दिशा में प्रयास-
ज्योतिबा ने महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का समर्थन किया था। उस समय की कुछ साक्षर महिलाओं में से एक, सावित्रीबाई को उनके पति ज्योतिराव ने पढ़ना और लिखना सिखाया था।
1851 में, ज्योतिबा ने लड़कियों के स्कूल की स्थापना की और अपनी पत्नी को स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए कहा। बाद में, उन्होंने लड़कियों के लिए दो और स्कूल खोले और निचली जातियों के लिए एक स्वदेशी स्कूल, विशेष रूप से महार और मंगल के लिए।
ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थितियों का एहसास किया और युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए।
अपने समय के आसपास, समाज एक पितृसत्तात्मक था और महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से घृणित थी। महिला शिशुहत्या एक सामान्य घटना थी और इसलिए बाल विवाह होता था, बच्चों के साथ कभी-कभी पुरुषों की शादी ज्यादा उम्र की होती थी। ये महिलाएं अक्सर युवा होने से पहले ही विधवा हो जाती थीं और उन्हें बिना किसी पारिवारिक समर्थन के छोड़ दिया जाता था। ज्योतिबा को उनकी दुर्दशा से पीड़ा हुई और उन्होंने 1854 में समाज के क्रूर हाथों को नष्ट होने से बचाने के लिए एक अनाथालय की स्थापना की।
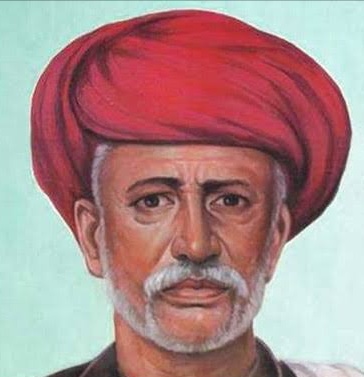
जाति भेदभाव के उन्मूलन के प्रयास-
ज्योतिराव ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों पर हमला किया और उन्हें "पाखंडी" करार दिया। उन्होंने उच्च जाति के लोगों के अधिनायकवाद के खिलाफ अभियान चलाया और उन पर लगे प्रतिबंधों को धता बताने के लिए "किसानों" और "सर्वहारा" का आग्रह किया।
उन्होंने सभी जातियों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए अपना घर खोला। वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में शामिल करके उनकी मान्यताओं का अनुकरण किया। उनका मानना था कि राम जैसे धार्मिक प्रतीकों को ब्राह्मण द्वारा निचली जाति को वश में करने के लिए लागू किया जाता है।
ज्योतिराव की गतिविधियों पर समाज के रूढ़िवादी ब्राह्मण उग्र थे। उन्होंने उसे समाज के मानदंडों और नियमों को दरकिनार करने के लिए दोषी ठहराया। कई ने उन पर ईसाई मिशनरियों की ओर से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। लेकिन ज्योतिराव दृढ़ थे और उन्होंने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिराव को कुछ ब्राह्मण मित्रों का समर्थन प्राप्त था जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना समर्थन दिया।
सत्यशोधक समाज-
1873 में, ज्योतिबा फुले ने सत्य षोधक समाज (सत्य के साधकों का समाज) का गठन किया। उन्होंने मौजूदा मान्यताओं और इतिहास को व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया, केवल एक समानता को बढ़ावा देने वाले संस्करण का पुनर्निर्माण किया। ज्योतिराव ने हिंदुओं के प्राचीन पवित्र ग्रंथ, वेदों की निंदा की। उन्होंने कई अन्य प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणवाद के इतिहास का पता लगाया और समाज में "शूद्रों" और "अतिशूद्रों" को दबाकर अपनी सामाजिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों को शोषक और अमानवीय कानूनों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य समाज को जातिगत भेदभाव से मुक्त करना था और ब्राह्मणों द्वारा प्रताड़ित कलंक से उत्पीड़ित निचली जाति के लोगों को मुक्त करना था। ज्योतिराव फुले ब्राह्मणों द्वारा निचली जाति और अछूत समझे जाने वाले सभी लोगों पर लागू करने वाले ’दलितों’ शब्द को बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। समाज की सदस्यता जाति और वर्ग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुली थी। कुछ लिखित अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने भी समाज के सदस्यों के रूप में यहूदियों की भागीदारी का स्वागत किया और 1876 तक 'सत्यशोधक समाज' ने 316 सदस्यों का घमंड कर दिया। 1868 में, ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामान्य स्नान टैंक का निर्माण करने का फैसला किया, जिसमें सभी मनुष्यों के प्रति उनका आलिंगनपूर्ण रवैया प्रदर्शित किया गया और उनकी जाति की परवाह किए बिना सभी के साथ भोजन करने की कामना की।
निधन:-
ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणों के शोषण से अछूतों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक होने के अलावा, वह एक व्यापारी भी थे। वह नगर निगम के लिए एक कृषक और ठेकेदार भी थे। उन्होंने 1876 और 1883 के बीच पूना नगर पालिका के आयुक्त के रूप में कार्य किया।
1888 में ज्योतिबा को आघात लगा और उन्हें लकवा मार गया। 28 नवंबर, 1890 को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले का निधन हो गया।
विरासत:-
महात्मा ज्योतिराव फुले की शायद सबसे बड़ी विरासत सामाजिक कलंक के खिलाफ उनकी सतत लड़ाई के पीछे की सोच है जो अभी भी काफी प्रासंगिक हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में, लोगों को इन भेदभावपूर्ण प्रथाओं को सामाजिक मानदंड के रूप में स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें बिना किसी सवाल के लागू करने की आवश्यकता थी, लेकिन ज्योतिबा ने जाति, वर्ग और रंग के आधार पर इस भेदभाव को बदलने की मांग की। वह सामाजिक सुधारों के लिए अनसुने विचारों के अग्रदूत थे। उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किया जो अंततः डॉ बी आर अम्बेडकर और महात्मा गाँधी, बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल करने वाले दिग्गज थे।
स्मरणोत्सव:-
1974 में धनजीय कीर द्वारा ज्योतिबा की एक जीवनी, जिसका शीर्षक था, महात्मा ज्योतिबा फुले: हमारे सामाजिक क्रांति के जनक ’हैं। पुणे में महात्मा फुले संग्रहालय महान सुधारक के सम्मान में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायिनी योजना की शुरुआत की जो गरीबों के लिए एक कैशलेस उपचार योजना है। महात्मा की कई मूर्तियों के साथ-साथ उनके नाम के साथ कई सड़क के नाम और शैक्षिक संस्थानों को फिर से खड़ा किया गया है - जैसे। मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई के रूप में फिर से संगठित किया गया और महाराष्ट्र के राहुरी में महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ, महर्षि का नाम बदलकर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ रखा गया।
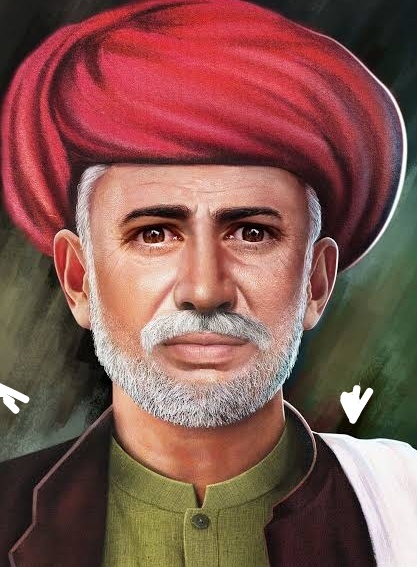
साहित्यिक रचना:-
ज्योतिबा ने अपने जीवनकाल में कई साहित्यिक लेखों और पुस्तकों को कलमबद्ध किया था और अधिकांश षट्कारायच आसुद ’जैसे सामाजिक सुधारों की उनकी विचारधारा पर आधारित थे। उन्होंने p तृतीया रत्न ’, ब्राहमंच कसाब’,। ईशारा ’जैसी कुछ कहानियाँ भी लिखीं। उन्होंने 'सत्सर' अंक 1 और 2 जैसे नाटक लिखे, जिन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उनके निर्देशों के तहत अधिनियमित किया गया था। उन्होंने सत्यशोधक समाज के लिए किताबें भी लिखीं जो ब्राह्मणवाद के इतिहास से जुड़ी थीं और पूजा के नियमों को रेखांकित किया कि निचली जाति के लोगों को सीखने की अनुमति नहीं थी।

