आर्यभट्ट
जन्म: - 476 ईस्वी कुसुमपुर या अस्माक (पाटलिपुत्र)मृत्यु: - 550 ईस्वी
कार्य: -गणित, खगोलीय
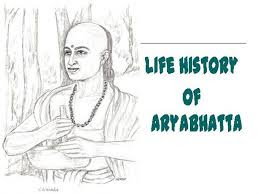
आज हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इसीलिए रात और दिन होते हैं। मध्ययुगीन काल में, 'निकोलस कोपरनिकस' ने इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य से अवगत होंगे कि 'कोपरनिकस' से लगभग 1 हजार साल पहले, आर्यभट्ट ने पाया था कि पृथ्वी गोल है और इसकी परिधि लगभग 24835 है। मीलों दूर है। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म के विश्वास को गलत साबित किया। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को भी पता था कि चंद्रमा और अन्य ग्रह सूर्य की किरणों से प्रकाशित होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने स्रोतों से साबित किया कि एक वर्ष में 36.2 दिन नहीं बल्कि 365.2951 दिन होते हैं।

प्रारंभिक जीवन : -
आर्यभट्ट ने अपनी जन्मभूमि कुसुमपुर को अपनी पुस्तक 'आर्यभटीय' और जन्म स्थान शक संवत 398 (476) में लिखा है। इस जानकारी के साथ उनके जन्म का वर्ष निर्विवाद है लेकिन वास्तविक जन्मस्थान के बारे में विवाद है। कुछ स्रोतों के अनुसार, आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अश्मक क्षेत्र में हुआ था और यह निश्चित है कि अपने जीवन के किसी समय में वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय तक वहाँ भी रहे थे। सातवीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने हिंदू और बौद्ध परंपराओं के साथ कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) के रूप में की है। अध्ययन का एक बड़ा केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया गया था और यह संभव है कि आर्यभट्ट इसके साथ जुड़े रहे हों। यह संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वहाँ रहते थे। गुप्त काल को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है।
काम : -
आर्यभट्ट की रचनाएँ उनके द्वारा रचित ग्रंथों से आती हैं। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभटीय, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धान्त जैसे ग्रंथों की रचना की। 'आर्यभट्ट सिद्धांत' के बारे में विद्वानों में बहुत अंतर है। यह माना जाता है कि सातवीं शताब्दी में 'आर्यभट्ट सिद्धांत' का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। वर्तमान में इस पुस्तक के केवल 34 छंद उपलब्ध हैं और विद्वानों को इस बात की कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि इस तरह की उपयोगी पुस्तक कैसे गायब हो गई है।

आर्यभटीय: -
आर्यभटीय उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष वर्णन प्रदान करता है। यह माना जाता है कि आर्यभट्ट ने स्वयं इसे यह नाम नहीं दिया होगा, लेकिन बाद में टीकाकारों ने आर्यभटीय नाम का उपयोग किया होगा। इसका उल्लेख भास्कर प्रथम ने भी किया है, जो आर्यभट्ट के शिष्य हैं। इस पुस्तक को कभी-कभी आर्य-शत-अष्ट (अर्थात आर्यभट्ट के 108 - अपने पाठ में छंदों की संख्या) के रूप में भी जाना जाता है। आर्यभटीय में वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रृंखला और विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। वास्तव में, यह पुस्तक गणित और खगोल विज्ञान का संग्रह है। आर्यभटीय के गणितीय भाग में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति और गोलाकार त्रिकोणमिति शामिल हैं। इसमें निरंतर अंश, द्विघात समीकरण, विद्युत श्रृंखला का योग (शक्ति श्रृंखला का योग) और साइन की एक तालिका शामिल है। आर्यभटीय में कुल 108 छंद हैं, साथ ही 13 परिचयात्मक जोड़ भी हैं।
इसे चार शब्दों या अध्यायों में बांटा गया है: -
1. गीत उत्पाद
2. गणित
3. क्रोनोग्राम
4. गोलपाद
आर्य सिद्धांत: -
आर्य-सिद्धान्त खगोलीय गणनाओं से ऊपर का एक कार्य है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह पुस्तक अब विलुप्त हो चुकी है और इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है, वह या तो वराहमिहिर के लेखन, आर्यभट्ट के समकालीन या बाद के गणितज्ञों और टिप्पणीकारों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम आदि के कार्यों से है। इस पुस्तक के बारे में हमें जो भी जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर, ऐसा लगता है कि यह कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित है और यह आर्यभटीय के सूर्योदय के बजाय मध्यरात्रि की गणना का उपयोग करता है। इस पुस्तक में कई खगोलीय उपकरणों का भी वर्णन किया गया है। उनमें से मुख्य हैं शंकु-यंत्र, छाया-यंत्र, संभवतः कोण-मापक यंत्र, धनुर-यन्त्र / चक्र-यन्त्र, एक बेलनाकार छड़ी यति-यन्त्र, छत्र-यन्त्र और जल घड़ियाँ।
उनके द्वारा एक तीसरी पुस्तक भी उपलब्ध है लेकिन यह मूल रूप में नहीं बल्कि अरबी अनुवाद - अल एनटीएफ या अल नन्फ के रूप में मौजूद है। यह पुस्तक आर्यभट्ट की पुस्तक का अनुवाद होने का दावा करती है, लेकिन इसका वास्तविक संस्कृत नाम अज्ञात है। यह फारसी विद्वान और इतिहासकार अबू रेहान अल-बिरूनी द्वारा नोट किया गया है।
आर्यभट्ट का योगदान: -
आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आर्यभट्ट ने ज्योतिष और संबंधित गणित के सिद्धांत को 120 आर्यखंडों में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आर्यभटीय' में प्रस्तुत किया है।
उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज की तुलना में अधिक सटीक रूप से 'पाई' के मूल्य का प्रतिनिधित्व किया और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार यह घोषित किया गया कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है।
आर्यभट्ट के कार्यों में स्थान-मूल्य अंक प्रणाली स्पष्ट रूप से मौजूद थी। यद्यपि उन्होंने शून्य को इंगित करने के लिए किसी भी प्रतीक का उपयोग नहीं किया था, गणितज्ञों का मानना है कि दस की शक्ति के लिए एक स्थान धारक के रूप में शून्य का ज्ञान एक खाली गुणांक के साथ आर्यभट्ट के स्थान-मूल्य अंक प्रणाली में निहित था।
यह आश्चर्य और आश्चर्य की बात है कि आज के उन्नत उपकरणों के बिना, उन्होंने लगभग डेढ़ हजार साल पहले ज्योतिष की खोज की थी। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले कोपरनिकस (1473 से 1543 ईस्वी) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की खोज की थी। "गोलपाद" में, आर्यभट्ट ने पहली बार साबित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
इस महान गणितज्ञ के अनुसार एक वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध 62,832: 20,000 है जो चार दशमलव स्थानों के लिए शुद्ध है। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार, पृथ्वी की परिधि 39,968.0582 किलोमीटर है, जो कि इसके वास्तविक मान 40,075.0167 किलोमीटर से केवल 0.2% कम है।


